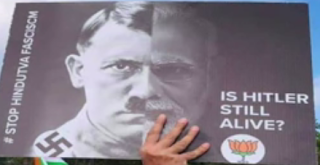26 दिसंबर:पूण्यतिथि विशेष
#जब_एक_युवती_द्वारा_चलायी_गयी_गोलियों_से_थर्रा_उठा_कलकत्ता_विश्वविद्यालय
6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्व विद्यालय के कनवोकेशन हाल में दीक्षांत समारोह में सैकड़ों लोग एक युवती द्वारा लगातार चलायी जा रही गोलियों से स्तब्ध रह गए.उस युवती केनिशाने पर बंगाल का तत्कालीन गवर्नर स्टेनले जैक्सन था.जैक्सन के अपने निकट पहुँचते ही उस पर उस युवती ने एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दीं.
हालांकि दुर्भाग्य से जैक्सन बच गया और बीना दास को गिरफ्तार कर 9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दीगयी.
उस दीक्षांत समारोह में गोली चलानेवाली क्रान्तिकारी और राष्ट्रवादी विचारों से ओत प्रोत वो युवती थी वीणा दास.वह अन्य स्नातकों के साथ दीक्षांत समारोह में थी.1937 में प्रान्तों में कोंग्रेसी सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियो के साथ बीना भी जेल से बाहर आ गयी.भारत छोड़ो आन्दोलन” के समय उन्हें तीन वर्ष केलिए नजरबंद कर लिया गया था.1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्य रही . गांधीजी की नौआखाली यात्रा के समय लोगो के पुनर्वास के काम में बीना (Bina Das) ने भी आगे बढकर भाग लिया .
बंगाल के कृष्णानगर में 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्द ब्रह्मसमाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाजसेविका सरला देवी के घर पर जन्मीं .बीना दास अपने अध्ययन काल में ही अंग्रेजों के खिलाफ निकाले जाने वाले विरोध मार्चों और रैलियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी.1947 में उनका युगान्तर समूह के भारतीय स्वतन्त्रता कार्यकर्ता जतीश चन्द्र भौमिक से विवाह हो गया.पति के देहान्त के बाद उन्होंने ऋषिकेश में एकान्त जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया और अज्ञातवास में ही 26 दिसंबर 1986 को मृत्यु को प्राप्त किया.
Sunil Singh
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2771784572843660&set=a.856456391043164&type=3
~विजय राजबली माथुर ©